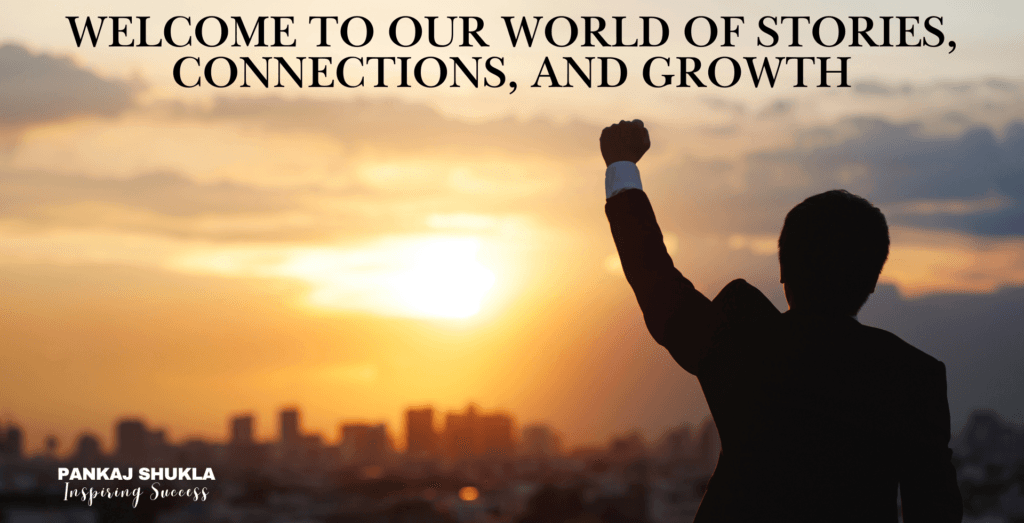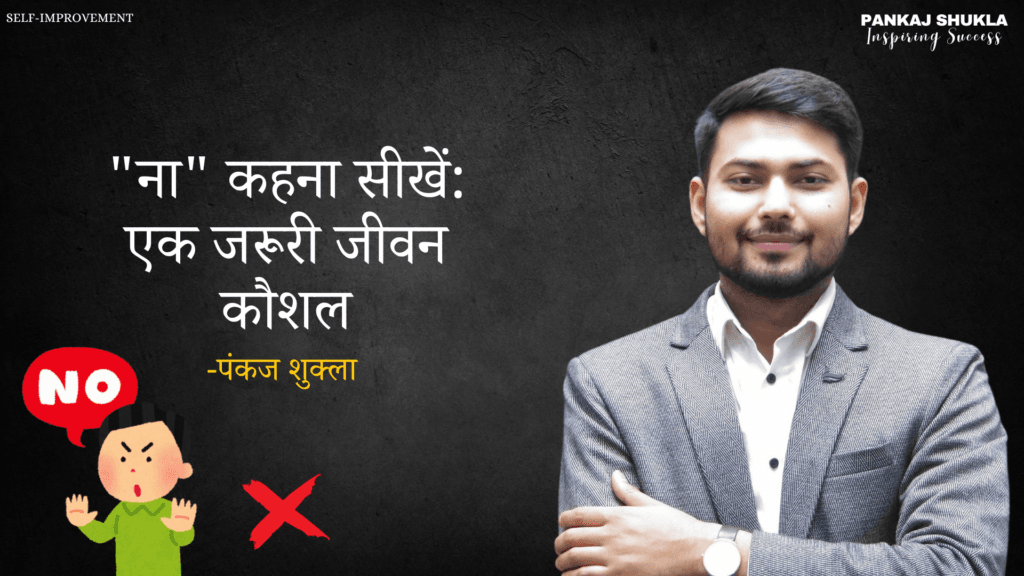नमस्ते,
मैं पंकज शुक्ला, आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की उस यात्रा के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसने मुझे पूरी तरह से बदलकर रख दिया। यह किसी मंज़िल तक पहुँचने की नहीं, बल्कि ख़ुद को पाने की कहानी है।
कुछ साल पहले तक, मैं भी ज़िंदगी की एक अनजानी दौड़ में भागे जा रहा था। लक्ष्य तय थे, रास्ते बने-बनाए थे और दिमाग़ बस उन रास्तों पर दौड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया था। ज़िंदगी एक चेकलिस्ट की तरह थी—ये करना है, वो हासिल करना है। मैं चीज़ों को जानता था, समझता था, पर शायद ‘महसूस’ नहीं करता था। मेरी दुनिया सही और ग़लत, सफलता और असफलता के दो किनारों में बंटी हुई थी।
और फिर, मेरी ज़िंदगी में दर्शनशास्त्र (Philosophy) का प्रवेश हुआ।
सच कहूँ तो शुरुआत में यह मेरे लिए बस कुछ विचारकों और उनके जटिल सिद्धांतों का संग्रह था। लेकिन जैसे-जैसे मैंने पन्ने पलटने शुरू किए, मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई किताब नहीं, बल्कि अपनी ही ज़िंदगी का आईना पढ़ रहा हूँ।
Table of Contents
वह पहला पल, जब सोच पर जमी धूल हटी
मुझे आज भी याद है जब मैंने प्लेटो की ‘गुफा का सिद्धांत’ (Allegory of the Cave) पढ़ा। पढ़ते-पढ़ते मैं आश्चर्यचकित रह गया। मुझे लगा कि मैं भी तो उसी गुफा का एक कैदी हूँ, जो दीवारों पर बनती परछाइयों को ही असली दुनिया मान बैठा है। ज्ञान का सूरज, सत्य की रोशनी तो इस गुफा के बाहर है। उस एक विचार ने मेरे सालों के विश्वास को हिलाकर रख दिया।
फिर सुकरात (Socrates) से मुलाक़ात हुई, जिन्होंने कहा, “एक ही चीज़ है जो मैं जानता हूँ, और वह यह है कि मैं कुछ नहीं जानता।” मेरे ‘ज्ञान’ का सारा अहंकार एक पल में चूर-चूर हो गया। यह मेरे बदलाव की शुरुआत थी। यह वह पल था जब मैंने रटना छोड़कर, सच में सोचना शुरू किया।
कैसे बदला मेरा सोचने, काम करने और जीने का नज़रिया
दर्शन महज़ सिद्धांतों का मकड़जाल नहीं है; यह जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। इसने मेरे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के हर पहलू को छुआ और उसे एक नया आयाम दिया। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया, बल्कि विचारों की परत-दर-परत मेरे व्यक्तित्व पर चढ़ती गई।
1. सोच का रूपांतरण: “क्यों” और “कैसे” की क्रांति
पहले मैं एक ऐसी नाव की तरह था, जिसे लहरें जहाँ चाहें, ले जाती थीं। समाज, परिवार और परिवेश द्वारा दी गई धारणाएं ही मेरी सच्चाई थीं। दर्शन ने मुझे उस नाव का पतवार थमा दिया।
- संदेह की पवित्रता (The Sanctity of Doubt): रेने देकार्त (René Descartes) के “Cogito, ergo sum” (मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ) ने मुझे सिखाया कि अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण ‘सोचने’ की क्षमता है। उन्होंने हर उस चीज़ पर संदेह किया जिस पर संदेह किया जा सकता था, ताकि वो एक असंदिग्ध सत्य तक पहुँच सकें। मैंने भी अपनी मान्यताओं पर संदेह करना सीखा। क्या जो मैं मानता हूँ, वो सच में मेरा अपना विचार है या किसी और का दिया हुआ? इस प्रक्रिया ने मेरे दिमाग़ से बहुत सारा वैचारिक कचरा साफ़ कर दिया।
- सत्य की बहुआयामी प्रकृति: मैं दुनिया को सही और ग़लत के दो खेमों में बांटकर देखता था। लेकिन जैन दर्शन के ‘अनेकांतवाद’ और ‘स्याद्वाद’ ने मेरी इस संकीर्ण दृष्टि को तोड़ दिया। उन्होंने सिखाया कि सत्य एक हाथी की तरह है और हम सब अंधे व्यक्तियों की तरह उसके अलग-अलग अंगों को छूकर उसे परिभाषित कर रहे हैं। कोई पैर को खंभा कह रहा है, कोई पूंछ को रस्सी। सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन आंशिक रूप से। इस समझ ने मुझे बौद्धिक रूप से विनम्र और दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णु बनाया। अब मैं यह नहीं कहता कि “तुम ग़लत हो,” बल्कि पूछता हूँ, “तुम ऐसा क्यों सोचते हो?”
2. भावनाओं का प्रबंधन: मन की शांति का विज्ञान
मैं हमेशा मानता था कि भावनाएँ अनियंत्रित होती हैं और हम उनके रहमोकरम पर जीते हैं। लेकिन दर्शन ने मुझे भावनाओं का मालिक बनना सिखाया।
- बौद्ध दर्शन और इच्छाओं का गणित: महात्मा बुद्ध के ‘चार आर्य सत्य’ ने मुझे जीवन के दुखों का मूल कारण समझाया—तृष्णा (इच्छा)। जब तक हम चीज़ों, लोगों और परिणामों से चिपके रहते हैं, दुख निश्चित है। मैंने सीखा कि खुशी कुछ पाने में नहीं, बल्कि जो है, उसे स्वीकार करने और अनावश्यक इच्छाओं को त्यागने में है। यह वैराग्य नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता है। इसने मुझे छोटी-छोटी बातों पर विचलित होने से बचाया और एक अद्भुत मानसिक शांति दी।
- स्टोइक दर्शन (Stoicism) और नियंत्रण का दायरा: एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस जैसे स्टोइक विचारकों ने मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया—उन चीज़ों के बीच अंतर करना जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूँ और जिन्हें नहीं। मैं मौसम, दूसरे लोगों के व्यवहार या किसी अप्रत्याशित घटना को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ अपने प्रयासों, अपने विचारों और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता हूँ। यह अहसास होते ही मेरे जीवन से 90% चिंताएँ भाप बनकर उड़ गईं। अब मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ़ उन चीज़ों पर लगाता हूँ जो मेरे वश में हैं।
3. कर्म का दर्शन: उत्कृष्टता की साधना
दर्शन ने मेरे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। अब काम केवल एक ज़रूरत नहीं, बल्कि आत्म-अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है।
- गीता का ‘निष्काम कर्म’: प्रक्रिया में डूब जाना: श्रीमद्भगवद्गीता का यह सिद्धांत मेरे लिए जीवन रक्षक साबित हुआ। “कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं।” यह महज़ एक वाक्य नहीं, तनाव मुक्ति का सूत्र है। जब मैंने अपना ध्यान फल की चिंता से हटाकर कर्म की गुणवत्ता पर लगाया, तो चमत्कार हो गया। काम बोझ नहीं, एक खेल बन गया। मैं उस प्रक्रिया में इतना डूबने लगा कि समय का पता ही नहीं चलता था। उत्कृष्टता अपने आप आने लगी, क्योंकि अब कोई दबाव नहीं था, सिर्फ़ कर्म का आनंद था।
- अरस्तू का ‘यूडेमोनिया’ (Eudaimonia): अरस्तू के अनुसार, जीवन का परम लक्ष्य ‘यूडेमोनिया’ है, जिसे अक्सर ‘खुशी’ अनुवादित किया जाता है, लेकिन इसका सही अर्थ है ‘मानव क्षमताओं का पूर्ण विकास’ या ‘उत्कर्ष की अवस्था’। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख इंद्रिय सुख में नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानकर उन्हें उत्कृष्टता के साथ अभ्यास करने में है। इसने मुझे अपने हर कार्य को—चाहे वह पढ़ाई हो, कोई हॉबी हो या किसी से बातचीत—पूरी लगन और उत्कृष्टता के साथ करने के लिए प्रेरित किया।
4. रिश्तों का नवीनीकरण: मानवता से गहरा जुड़ाव
मैं अक्सर लोगों को उनके कार्यों से जज करता था। दर्शन ने मुझे सतह के नीचे झाँकना सिखाया।
- कांट का मानवता का सिद्धांत: इम्मैन्युअल कांट ने कहा कि हर मनुष्य को हमेशा एक ‘साध्य’ (End) मानना चाहिए, कभी भी केवल एक ‘साधन’ (Means) नहीं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का सम्मान उसके अपने अस्तित्व के लिए होना चाहिए, न कि इसलिए कि वह हमारे किसी काम आ सकता है। इस एक विचार ने मेरे देखने का नज़रिया बदल दिया।
- सर्वपल्ली राधाकृष्णन का समन्वय: भारत के इस महान दार्शनिक राष्ट्रपति ने सिखाया कि कैसे अलग-अलग विचार और संस्कृतियाँ एक साथ शांति से रह सकती हैं। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दर्शन के बीच पुल बनाया। उनके विचारों ने मुझे सिखाया कि विविधता टकराव का कारण नहीं, बल्कि समृद्धि का स्रोत है। इसने मेरे दिल और दिमाग़ के दरवाज़े दुनिया के लिए खोल दिए।
5. स्वतंत्रता के सही अर्थ की खोज
पहले मेरे लिए आज़ादी का मतलब था – कोई रोक-टोक न होना। लेकिन अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्यां-पॉल सार्त्र (Jean-Paul Sartre) ने जब कहा कि “मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है” (Man is condemned to be free), तो मैं इस सोच से सिहर उठा। उन्होंने समझाया कि हम अपने जीवन का अर्थ बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और अकेले जिम्मेदार हैं। हम अपनी परिस्थितियों या अतीत का बहाना नहीं बना सकते। यह अहसास जितना डरावना था, उससे कहीं ज़्यादा आज़ाद करने वाला था। मैंने पहली बार समझा कि असली स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर चुनाव की जिम्मेदारी लेने और अपने मूल्यों को ख़ुद गढ़ने में है।
6. अस्तित्व के केंद्र की यात्रा: उपनिषदों का महावाक्य
अब तक की यात्रा मन, बुद्धि और व्यवहार को बदलने की थी। लेकिन उपनिषदों ने मुझे अस्तित्व के उस मूल प्रश्न पर लाकर खड़ा कर दिया – “मैं कौन हूँ?” (कोऽहम्?)। मैं खुद को पंकज शुक्ला मानता था – यह शरीर, ये विचार, ये भावनाएँ, ये सफलताएँ और असफलताएँ।
लेकिन उपनिषदों ने मुझे ‘नेति-नेति’ (यह नहीं, यह नहीं) की प्रक्रिया सिखाई। मैं यह शरीर नहीं हूँ, क्योंकि यह बदलता है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। मैं ये विचार नहीं हूँ, क्योंकि ये आते-जाते रहते हैं। मैं ये भावनाएँ नहीं हूँ, क्योंकि ये भी क्षणिक हैं। तो फिर मैं कौन हूँ?
इस खोज की गहराई में मुझे उपनिषदों का महावाक्य मिला – “अहं ब्रह्मास्मि” (मैं ही ब्रह्म हूँ)। यह अहंकार की घोषणा नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। इसका अर्थ यह समझना है कि मेरी व्यक्तिगत चेतना (आत्मा) उस परम सार्वभौमिक चेतना (ब्रह्म) का ही अंश है, उससे अलग नहीं। जैसे एक बूंद को यह एहसास हो जाए कि वह सागर से अलग नहीं, बल्कि सागर ही है। इस एक अनुभूति ने मेरे अस्तित्व के सारे समीकरण बदल दिए। अकेलेपन का भाव मिट गया, क्योंकि जब सब कुछ उसी एक चेतना का विस्तार है, तो पराया कौन है? मृत्यु का भय कम हो गया, क्योंकि जो सनातन है, उसका अंत कैसे हो सकता है?
7. स्थितप्रज्ञ की अवस्था: सुख-दुःख से परे का जीवन
यह शायद दर्शन के अध्ययन का सबसे बड़ा उपहार था। पहले मेरा जीवन एक पेंडुलम की तरह था—सफलता मिलने पर सुख के शिखर पर और असफलता मिलने पर दुःख के गर्त में। मैं बाहरी परिस्थितियों का गुलाम था। लेकिन जब मैंने श्रीमद्भगवद्गीता में ‘स्थितप्रज्ञ’ (स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति) के आदर्श को समझा, तो जीवन का लक्ष्य ही बदल गया।
भगवान कृष्ण कहते हैं: “दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥”
(अर्थात: जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुखों की लालसा नहीं करता और जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है।)
यह पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि असली जीत किसी परिणाम को हासिल करने में नहीं, बल्कि मन की उस अवस्था को पाने में है जो परिणाम से प्रभावित ही न हो। यह भावशून्य होना नहीं है, बल्कि भावों का स्वामी बनना है। अब मेरा प्रयास ‘खुशी खोजने’ का नहीं, बल्कि ‘शांति और संतुलन’ स्थापित करने का होता है। यह एक सतत अभ्यास है, पर इसने मुझे जीवन के थपेड़ों के बीच भी स्थिर रहना सिखा दिया है।
आज का पंकज: एक आज़ाद विचारक
यह बदलाव एक बौद्धिक व्यायाम मात्र नहीं था, यह मेरे अस्तित्व की गहराइयों में उतर रहा था। जिस पंकज को मैं जानता था, वह परत-दर-परत पिघल रहा था, और एक नया, अधिक शांत, अधिक विचारशील और अधिक करुणामय व्यक्तित्व आकार ले रहा था।
आज जब मैं आईने में देखता हूँ, तो मुझे एक नया पंकज दिखाई देता है। यह वो इंसान है जो अनिश्चितता से डरता नहीं, बल्कि उसमें संभावनाएं देखता है। यह वो इंसान है जो जवाबों से ज़्यादा अच्छे सवालों से प्रेम करता है। इसने सीखा है कि असली विकास अपनी सीमाओं को जानने और उन्हें विनम्रता से स्वीकार करने में है।
दर्शन ने मुझे कोई बना-बनाया नक्शा नहीं दिया, बल्कि एक कंपास थमा दिया है, जिससे मैं अपने जीवन के किसी भी अनजान रास्ते पर दिशा खोज सकता हूँ।
निष्कर्ष
अक्सर हम दुनिया को समझने के लिए बाहर की ओर देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं। लेकिन दर्शनशास्त्र ने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ी खोज अपने भीतर की यात्रा है।
मैं एक विषय को समझने निकला था, और अंत में उस विषय ने मुझे मुझसे ही मिला दिया। और यक़ीन मानिए, इस मुलाक़ात से सुंदर और कुछ भी नहीं है।
यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। दर्शन एक अथाह सागर है और मैंने तो अभी कुछ ही मोतियों को छुआ है। और भी कई महत्वपूर्ण सीखें हैं, जिन्हें मैं भविष्य में आपके साथ साझा करता रहूँगा। लेकिन ज्ञान को जानना एक बात है और उसे जीना दूसरी। अभी तो मेरा सबसे बड़ा प्रयास इन्हीं सीखों को अपने आचरण और व्यवहार का सहज हिस्सा बनाने का है, यह एक सतत साधना है।
यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। यह उस हर साधक की कहानी हो सकती है, जो ज्ञान के इस महासागर में एक डुबकी लगाने की हिम्मत करता है।